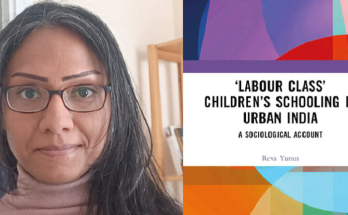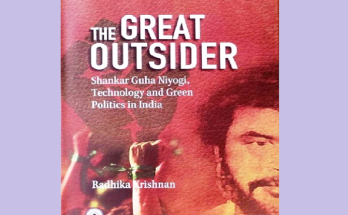By मनीष आज़ाद
1960 से पहले डाक्यूमेंट्री यानी ‘दस्तावेजी फ़िल्मों’ में उतना काम नहीं था। ज़्यादातर सरकार के सहयोग से उसी तरह की डाक्यूमेंट्री बनती थी, जो पहले आप पिक्चर हाल में फ़िल्म शुरू होने से पहले देखते थे।
हालाँकि इसी दौरान सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक जैसे लोगों ने कुछ अच्छी डाक्यूमेंट्री बनायी। मृणाल सेन ने ‘लेनिन’ पर एक डाक्यूमेंट्री बनाई थी।
लेकिन उसे राजनीतिक डाक्यूमेंट्री नहीं कह सकते। इस समय स्वतंत्र डाक्यूमेंट्री मेकर के रूप में जो बड़ा नाम आता है वह है ‘एस।
सुखदेव’ का. एस. सुखदेव नेहरु से बहुत प्रभावित थे। इन्होने बहुत सी फ़िल्में बनाई हैं। 1979 में उनकी मृत्यु हो गयी थी। वे अंत तक नेहरू के ही प्रभाव में रहे।
फिर भी नक्सल आन्दोलन से पहले की उनकी फ़िल्में और नक्सल आन्दोलन के बाद की उनकी फ़िल्मों में आप एक खास अन्तर पाएंगे।
ये भी पढ़ें-
- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव- Part-1
- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव : मलयालम सिनेमा Part-2

आनंद पटवर्धन
नक्सल आन्दोलन के बाद की उनकी एक फ़िल्म में वे बोलते है- “सिद्धार्थ तुमने एक बीमार को देखा, एक रोगी को देखा, एक बूढ़े को देखा तो तुमने दुनिया छोड़ दी, यहाँ आओ तो तुम्हें दिखेगा कि कितने बीमार हैं, कितने रोगी हैं, कितने बेसमय मर जा रहे हैं, अब तुम कहाँ जाओगे”।
सत्यजीत रे, एस सुखदेव जैसे लोग सीधे-सीधे नक्सल आन्दोलन से प्रभावित नहीं थे। लेकिन चूँकि ये सच्चे कलाकार थे, इसलिए जब ये कलाकार असल जीवन को ‘कैप्चर’ करते थे तो उनकी फ़िल्मों में वह बदला हुआ यथार्थ आता ही था।
1970 के बाद डाक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग में जो सबसे बड़ा नाम है, वह है ‘आनंद पटवर्धन’ का।
आनंद पटवर्धन सीधे–सीधे लैटिन अमेरिकन डाक्यूमेंट्री मेकर की तरह, फ़िल्में बनाना, फ़िल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करना, और फ़िल्म को एक क्रांतिकारी हथियार की तरह इस्तेमाल करना, इसी कांसेप्ट (concept) के साथ फ़िल्म बनाते हैं।
ये भी पढ़ें-
- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव : बांग्ला फ़िल्में Part-3
- समानांतर सिनेमाः गैर तेलुगु लोगों द्वारा बनाई गईं तेलुगु फ़िल्में : Part-4

तकनीक का इस्तेमाल
उन्होंने जेपी आन्दोलन पर बेहतरीन फ़िल्म बनाई थी- ‘वेव्स ऑफ़ रेवोलुशन’ (Waves of Revolution)। 1978 में ‘प्रिज़नर ऑफ़ कांसंस’ (Prisoners of Conscience) बनाई। उसमें ‘मेरी टायलर’ का एक इंटरव्यू है।
वह बताती हैं कि नक्सलियों को किस तरह से पकड़ा और टॉर्चर किया जाता था। एक घटना का जिक्र करती हुई वो कहती हैं कि एक गांव में एक नक्सली को टॉर्चर करते हुए ‘इलेक्ट्रिक शॉक’ दिए गए।
जबकि उस गांव में बिजली नहीं थी। यानी सरकार गांव में बिजली नहीं दे पा रही है लेकिन उसी गांव में नक्सलियों को ‘इलेक्ट्रिक शॉक’ दिया जा रहा है।
आनंद पटवर्धन की दूसरी खूबी यह है कि वह सोवियत रूस के ‘आइजेन्स्टीन’ (Sergei Eisenstein) के ‘मोन्ताज़ थियरी’ का ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं।
इसी फ़िल्म में जब आदिवासी क्रांतिकारी ‘किस्ता गौड’ को फांसी दी जा रही है तो दूसरे ही सीन में ‘रिपब्लिक डे’ परेड है। ड्रम बज रहा है, ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा’ गाया जा रहा है।
ये भी पढ़ें-
- थर्ड वर्ल्ड सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आन्दोलन का प्रभाव : हिंदी सिनेमा Part-5
- एक ज़रूरी फ़िल्म ‘चिल्ड्रेन ऑफ हैवेन’; मासूमियत की खुशबू के 25 साल
संजय काक
1985 में उनकी एक और डाक्यूमेंट्री फ़िल्म आई थी- ‘हमारा शहर’। यह एक बेहद ज़रूरी फ़िल्म है। फ्रेडरिक एंगल्स ने जिसे ‘सोशल वॉर’ कहा था, यह डाक्यूमेंट्री उसकी कहानी कहती है।
यह ‘सोशल वॉर’ मुम्बई में कैसे चल रहा है, उसे यह फ़िल्म बेहतरीन तरीके से ‘कैप्चर’ करती है। इसमे ‘गोदरेज समूह’ के मालिक गोदरेज का एक इंटरव्यू है।
गोदरेज कहते हैं- “इन सारे लोगों को फैक्ट्री में बुलाया जाय, काम करवाया जाय, और फिर पैक कर इनके घर भेज दिया जाय, इनको यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चूहे हैं, इनको इंसान की तरह रहने की आदत नहीं है”।
इसमें मुम्बई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ‘जे एफ़ रिबेरो’ का भी एक इंटरव्यू है।
जे.एफ़. रिबेरो बोलते हैं- ‘यदि इनको हम फुटपाथ से नहीं हटायेंगे, इनकी झुग्गी–झोपड़ियाँ नहीं तोड़ेंगे तो ये पहले हमारे सार्वजानिक जगहों पर कब्ज़ा करेंगे, फिर सड़क पर कब्ज़ा करेंगे, फिर एक दिन आपके हमारे घरों में आ जायेंगे। जैसे चीन और सोवियत रूस में हुआ’। यह रिबेरो का बयान है ऑन कैमरा।
ये ‘सोशल वार’ नहीं तो और क्या है। पूरी सीरीज है उनकी- ‘राम के नाम’, ‘युद्ध और शांति’, ‘हमारा शहर’, ‘जय भीम कामरेड’, ‘रीज़न’ आदि।
दूसरा महत्वपूर्ण नाम ‘संजय काक’ का है। वह 1986 से सक्रिय हैं। उनकी बहुत महत्वपूर्ण फ़िल्म ‘रेड एंट ड्रीम’ (Red Ant Dream) है। कश्मीर पर एक शानदार फ़िल्म ‘जश्ने आज़ादी’ बनाई।
ये भी पढ़ें-
- मट्टो की साइकिलः यह फिल्म हर मज़दूर को क्यों देखनी चाहिए?
- स्वतंत्रता आंदोलन के भुला दिए गए 15 नायक जिनसे कांपती थी अंग्रेज़ी हुकूमत: ‘द लास्ट हीरोज़’ का विमोचन
‘रेड एंट ड्रीम’ (Red Ant Dream) तो आज के नक्सल आन्दोलन पर है। यह सभी फ़िल्में उसी परंपरा में आती है, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है।
इसी समृद्ध परंपरा के कारण आज नए-नए फ़िल्मकार बेहद महत्वपूर्ण व उम्दा दस्तावेजी फ़िल्म बना रहे हैं।
अंत में फ़्रांस के मशहूर फ़िल्म समीक्षक, डाक्यूमेंट्री मेकर और ‘द सोसायटी ऑफ़ द स्पेक्टैकल’ (The Society of the Spectacle) के लेखक ‘गी दूबो’ (Guy Debord) की एक दिलचस्प व महत्वपूर्ण उद्धरण से मैं अपना यह लेख समाप्त करना चाहूँगा।
उन्होंने लिखा है- ‘दुनिया को फ़िल्माने का काम बहुत हुआ, असल सवाल उसे बदलने का है।’
(लेखक प्रगतिशील फ़िल्मों पर लिखते रहे हैं। विश्व सिनेमा, समानांतर सिनेमा और सामाजिक आंदोलन के अंतरसंबंध को मोटा मोटी समझने के लिए लिखा गया ये एक लंबा लेख है जिसे पांच हिस्सो में बांटा गया है और शृंखला में प्रकाशित होगा। इस लेख की यह अंतिम कड़ी है। )
ये भी पढ़ें-
- एक ज़रूरी फ़िल्म Mephisto: एक कलाकार जिसने अपनी आत्मा नाज़ियों को बेच दी
- घोड़े को जलेबी खिलाती और दर्शकों को Reality Trip कराती फ़िल्म
वर्कर्स यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए सब्स्क्रिप्शन ज़रूर लें- यहां क्लिक करें
(वर्कर्स यूनिटी के फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें। मोबाइल पर सीधे और आसानी से पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें।)